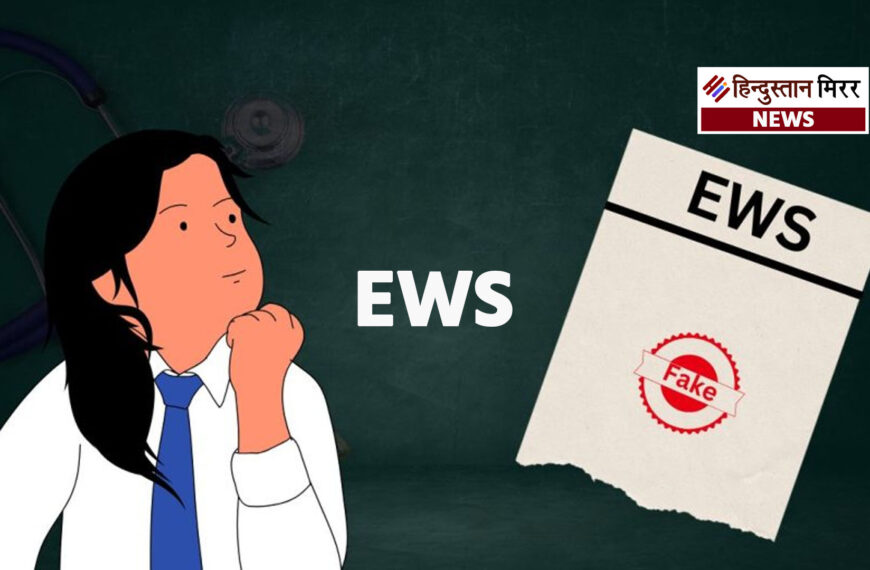1. तुलसी तुमने गाया – कृष्ण मुरारी पहारिया
तुलसी तुमने गाया
जागरण तभी आया
वह थी इतिहास की सुदीर्घ निशा, तम अपार
मरघट-सी नीरवता फैली थी आर-पार
प्रथम तुम्हारा ही स्वर था,
सुन पुरब अरूनाया
ऐसा था ताप तुम्हारी कविता के स्वर में
युग का युग जाग गया, बल आया नश्वर में
लड़ने को खड़ी हुई
तब जन-जन की काया
कटुता का जीवन से कुछ ऐसा योग हुआ
धरती पर आते ही दुख से संयोग हुआ
शिव बनकर पचा गए
जग ने जो भी ढाया
अपने सब त्याग गए, बोध नहीं जब जागा
किंतु सकल मानवता को तुमने अनुरागा
दिए रहे दलितों को
आदर्शों की छाया
राम की कथा में जो रावण की हार हुई
एक व्यवस्था थी जो जल-जलकर छार हुई
तुलसी तुम आए या
क्रांति-पर्व ही आया
पुस्तक : यह कैसी दुर्धर्ष चेतना (पृष्ठ 55) रचनाकार : कृष्ण मुरारी पहारिया प्रकाशन : दर्पण प्रकाशन संस्करण : 1998

2. नीलकंठ – राकेश मिश्र
कितने हैं
नीलकंठ
मेरी कपाल-अस्थियों में
कितनी बार मनाई
विजयादशमी
कितनी बार हो आया मैं
लंका
फिर भी
भटक जाते हैं
तलुओं से चले
धरती के शीतल संकेत
बार-बार
बार-बार।
पुस्तक : चलते रहे रात भर (पृष्ठ 26) रचनाकार : राकेश मिश्र प्रकाशन : राधाकृष्ण प्रकाशन संस्करण : 2019
3. एकमुखी दशानन – ओम् प्रकाश आदित्य
राम तो यहाँ पे अब नाम के ही रह गए हैं,
मर्यादा वाला नहीं किसी का चलन है,
ऋषिवत् कहीं एक भी न ऋषि मिलता है,
फल फूल रहा रिश्वत का चमन है।
नर होके बानर उछलते हैं कुर्सी पे,
भाई को जो छलते हैं ऐसे लछमन हैं,
दस मुख वाला तब एक ही दशानन था,
एक मुख वाले अब लाखों दशानन हैं।
पुस्तक : हास्य-व्यंग्य की शिखर कविताएँ (पृष्ठ 80) संपादक : अरुण जैमिनी रचनाकार : ओम् प्रकाश आदित्य प्रकाशन : राधाकृष्ण पेपरबैक्स संस्करण : 2013
4. विजयदशमी – गिरिजाकुमार माथुर
आसमान की आदिम छायाओं के नीचे,
दक्षिण का यह महासिंधु अब भी टकराता,
सेतुबंध की श्यामल, बहती चट्टानों से।
आँखों में, यह अंतरीप के मंदिर की चोटी उठती है,
जिस पर रोज़ साँझ छा जाते,
युग-युग रंजित, लाल, सुनहले, पीले बादल,
एक पुरातन तूफ़ानी-सी याद दिला कर,
जब, अविलंब, अग्नि-शर-चाप उठाते ही में,
नभ-चुंबी, काले पर्वत-सा ज्वाल मिटा था।
संस्कृतियों पर संस्कृतियों के महल मिट गए,
लौह नींव पर खड़े हुए गढ़, दुर्ग, मिनारें।
दृढ़ स्तंभ आधार भंग हो
गिरे, विभिन्न निशान, शास्ति के केतन डूबे।
महाकाल के भारी पाँवों से न मिट सके,
चित्रकूट, किष्किन्धा, नीलगिरी के जंगल,
पंचवटी की गुँथी हुई अलसायी छाँहें।
वाल्मीकि के मृत्युंजय स्वर ले अपने पर
सरयू, गोदावरी, नील, कृष्णा की धारा।
प्रेत-भरे इस यंत्रकाल में,
आज कोटि युग की दूरी से यादें आतीं,
शंभु-चाप से अविच्छिन्न इतिहास पुराने,
और वज्र-विद्युत से पूरित अग्नि-नयन वे
जिनमें भस्म हुए लंका-से पाप हज़ारों।
अब भी विजय-मार्ग में वह केतन दिखता है
लौट रहे उस मोर-विनिर्मित कुसुम-यान का,
लंबे-लंबे दुख-वियोग की अंतिम-वेला।
सीता के गोरे, काँटों से भरे चरण वे,
अग्नि-परीक्षाएँ पग-पग की;
घोर जंगलों, नदियों से जब पार उतरकर,
उन बिछुड़े नयनों का सुखमय मिलन हुआ था।
और चतुर्दश वर्षों पहले का प्रभात वह,
सुमन-सेज जब छोड़े तीन सुकुमार मूर्तियाँ,
तर, मंडित, वन-पथ पर चलीं तपस्वी बन कर,
राग-रंगीली दुनिया में आते ही आते
आसमान की आदिम छायाओं के नीचे
सेतुबंध से सिंधु आज भी टकराता है।
पदचिह्नों पर पदचिह्नों के अंक बन गए
कितने स्वर, ध्वनियाँ, कोलाहल डूब गए हैं।
किंतु सृजन की और मरण की रेखाओं में
चिर ज्वलंत निष्कंप एक लौ फिरती जाती,
धरती का तप जिस प्रकाश में पूर्ण हुआ है।
देश, दिशाएँ, काल लोक-सीमा से आगे,
वह त्रिमूर्ति चलती जाती मन के फूलों पर,
अपने श्यामल गौर चरण से पावन करती
वर्षों, सपुस्तक : तार सप्तक (पृष्ठ 155) संपादक : अज्ञेय रचनाकार : गिरिजाकुमार माथुर प्रकाशन : भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण : 2011दियों, युगों-युगों के इतिहासों को।

5. धारावाहिक – चंदन सिंह
धन्यवाद, श्रीराम!
रावण के वध के लिए, धन्यवाद! और
महँगाई के ज़माने में हमारे बच्चों को
तीर-धनुष एक मुफ़्त का खिलौना देने के लिए
धन्यवाद!
मशहरी लगाने वाली
बाँस की पुरानी लगभग विस्मृत फट्टियाँ
घर के अँधेरे में कहीं कोई पड़ी थीं
बरसों बाद उन्हें जगाया गया
और जैसे ही
लंबी नींद से जगने पर उनकी अँगड़ाई
धनुष के आकार की हुई
डोरियों से कसकर बाँध दिया गया उन्हें
हम सबकी ओर से, धन्यवाद!
बस, बच्चों की कुछ आँखों
कुछ अभागी गौरैयों
रंग बदलते हुए पकड़े जाने वाले
कुछ मूर्ख गिरगिटों को छोड़
हम सबकी ओर से, धन्यवाद!
ये निशाना बनेंगे तीर के
इन्हें लगेगी चोट
लेकिन इन्हें छोड़
हम सबकी ओर से
जो तीर के निशाने से बाहर रहेंगे
धन्यवाद!
धन्यवाद, श्रीराम!
धन्यवाद!
रचनाकार : चंदन सिंह प्रकाशन : हिन्दवी के लिए लेखक द्वारा चयनित
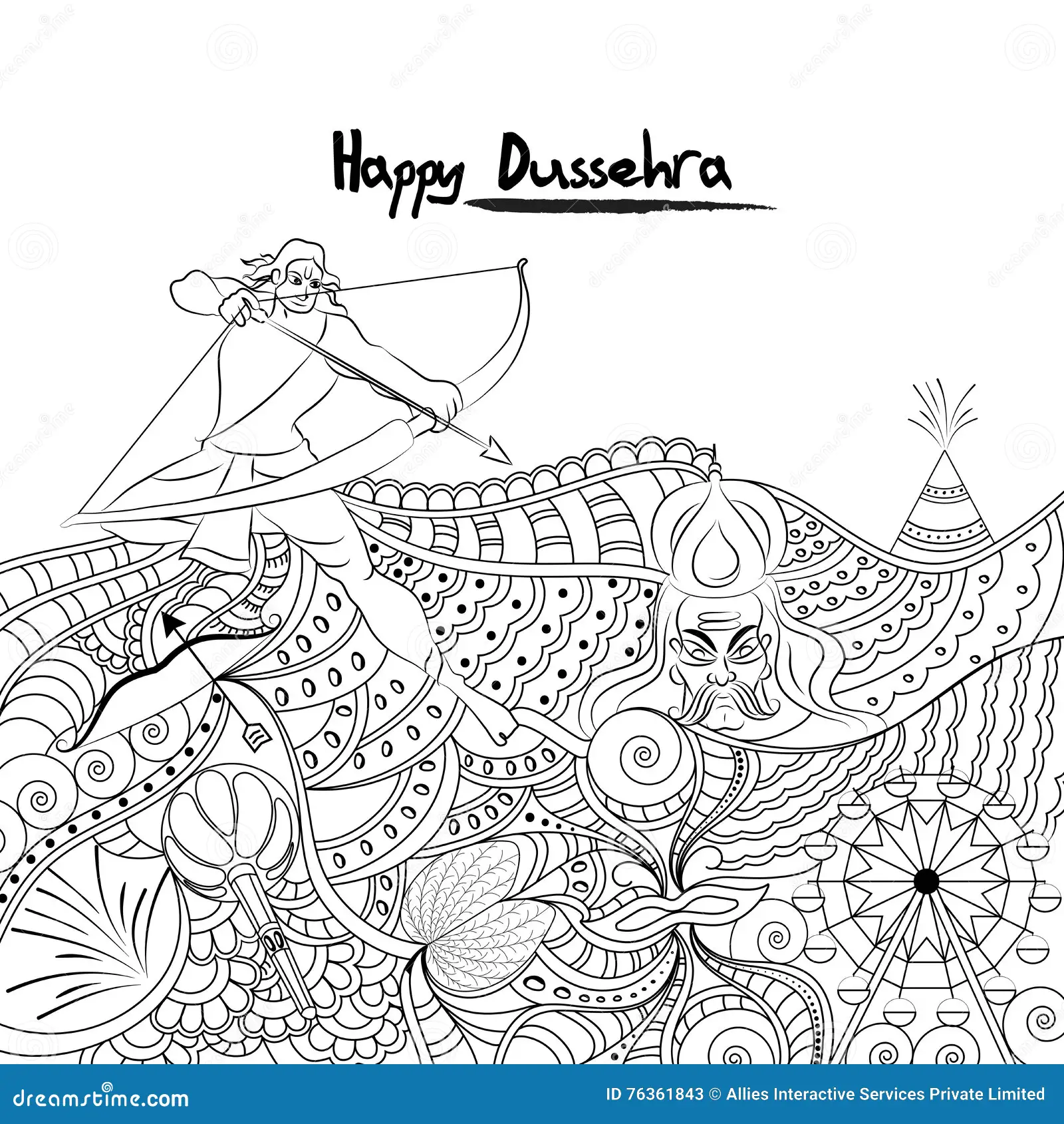
6. दिल और मन का रावण – वसीम अकरम
इस बार दशहरे में फिर
हम जलाएँगे रावण
शायद इस बार
भ्रष्टाचार रूपी रावण की बारी है
उसे जलाकर हम मनाएँगे जश्न
बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न।
बुराई के बजाय
बुराई के प्रतीक को जलाकर
कितना ख़ुश होते हैं हम
और अगली सुबह से ही
अपने कारोबार को फिर
जीने लगते हैं वैसे
जैसे रोज़ जिया करते थे इससे पहले,
शराब पीकर सड़क पर
बेवजह रिक़्शे वाले को डाँटकर
उसे अन्ना बनने का
बेवक़ूफ़ी भरा मशवरा दे डालते हैं।
ख़ुद में बुराई ढूँढ़ने की बजाय
दुनिया को बुरा कहने से
कभी नहीं हिचकते हम
कंधे पर गुनाहों की पोटली लिए
दर-ब-दर भटकते हैं
मगर दूसरे को गाली देने से
बाज़ नहीं आते कभी भी।
काग़ज़ी रावण तो
मर जाता है हर साल
मगर
हमारे ज़हनो-दिल में रोज़
जन्म लेता है एक रावण।
जिस दिन हम ख़ुद को
गाली देना सीख लेंगे
उस दिन हमारे दिल का रावण भी
मर जाएगा ख़ुद-ब-ख़ुद।
रचनाकार : वसीम अकरम प्रकाशन : हिन्दवी के लिए लेखक द्वारा चयनित

7. विजयदशमी – मैथिलीशरण गुप्त
जानकी जीवन, विजयदशमी तुम्हारी आज है,
दीख पड़ता देश में कुछ दूसरा ही साज है।
राघवेंद्र! हमें तुम्हारा आज भी कुछ ज्ञान है,
क्या तुम्हें भी अब कभी आता हमारा ध्यान है?
वह शुभ स्मृति आज भी मन को बनाती है हरा,
देव! तुम तो आज भी भूली नहीं है यह धरा।
स्वच्छ जल रखती तथा उत्पन्न करती अन्न है,
दीन भी कुछ भेंट लेकर दीखती संपन्न है॥
व्योम को भी याद है प्रभुवर तुम्हारी वह प्रभा!
कीर्ति करने बैठती है चंद्र-तारों की सभा।
भानु भी नव-दीप्ति से करता प्रताप प्रकाश है,
जगमगा उठता स्वयं जल, थल तथा आकाश है॥
दुःख में ही है! तुम्हारा ध्यान आया है हमें,
जान पड़ता किंतु अब तुमने भुलाया है हमें।
सदय होकर भी सदा तुमने विभो! यह क्या किया,
कठिन बनकर निज जनों को इस प्रकार भुला दिया॥
है हमारी क्या दशा सुध भी न ली तुमने हरे?
और देखा तक नहीं जन जी रहे हैं या मरे।
बन सकी हमसे न कुछ भी किंतु तुमसे क्या बनी?
वचन देकर ही रहे, हो बात के ऐसे धनी!
आप आने को कहा था, किंतु तुम आए कहाँ?
प्रश्न है जीवन-मरण का हो चुका प्रकटित यहाँ।
क्या तुम्हारा आगमन का समय अब भी दूर है?
हाय तब तो देश का दुर्भाग्य ही भरपूर है!
आग लगने पर उचित है क्या प्रतीक्षा वृष्टि की,
यह धरा अधिकारिणी है पूर्ण करुणा दृष्टि की।
नाथ इसकी ओर देखो और तुम रक्खो इसे,
देर करने पर बताओ फिर बचाओगे किसे?
बस तुम्हारे ही भरोसे आज भी यह जी रही,
पाप पीड़ित ताप से चुपचाप आँसू पी रही।
ज्ञान, गौरव, मान, धन, गुण, शील सब कुछ खो गया,
अंत होना शेष है बस और सब कुछ हो गया॥
यह दशा है इस तुम्हारी कर्मलीला भूमि की,
हाय! कैसी गति हुई इस धर्म-शीला भूमि की।
जा घिरी सौभाग्य-सीता दैन्य-सागर-पार है,
राम-रावण-वध बिना संभव कहाँ उद्धार है?
शक्ति दो भगवान् हमें कर्तव्य का पालन करे,
मनुज होकर हम न परवश पशु-समान जिएँ-मरें।
विदित विजय-स्मृति तुम्हारी यह महामंगलमयी,
जटिल जीवन-युद्ध में कर दे हमें सत्वर जयी॥
पुस्तक : मैथिलीशरण गुप्त ग्रंथावली-3 (पृष्ठ 67) संपादक : कृष्णदत्त पालीवाल रचनाकार : मैथिलीशरण गुप्त प्रकाशन : वाणी प्रकाशन संस्करण : 2008
8. दशहरा – नीलाभ अश्क
एक
एक जुलूस है, जो साल-दर-साल इसी तरह—
जगमगाते प्रकाश में,
खोई हुई प्रतिष्ठा की तलाश में,
दक्खिन से उत्तर चला जाता है—
गाता-बजाता,
अपने अंतर की पराजय को
लगातार झुठलाता।
दक्खिन से उत्तर
लौटती हुई हताश और थकी हुई
सेनाओं के पीछे-पीछे लौटता हुआ,
एक जला हुआ नगर अपने पीछे छोड़ता हुआ—
जहाँ अब कुछ भी बाक़ी नहीं है
हैरान आँखों के लिए।
न तो हड्डियों के सफ़ेद, चमकते हुए ढेर
न मँडराते गिद्ध, न ख़ून से भरे हुए तालाब
सिर्फ़ अनाम चिताओं की टोह में
बीते हुए दुःस्वप्न की खोह में
धीरे-धीरे रेंगती हुई,
बेहद हरी घास चढ़ आई है।
दो
यह सब उसके सामने है, उसके अंदर है,
जहाँ अब प्रेम और प्रतिष्ठा के बीच
संशय और निष्ठा के बीच
एक टूटता हुआ पुरुष है।
वही जानता है।
उसके भीतर कितना अवसाद है :
आग और रक्त के निर्णय को ठुकराता
अंतर के शून्य को गुँजाता
वही दुर्दम भय—लोकापवाद है।
क्यों वह भूल गया है,
कि बह, जो उसके इस नाटक की
विडंबना झेलती रही है
वही, छाया की तरह,
उसके साथ-सारे दुखों को हेलती रही है
दुख ही आमुख
दुख ही उसके जीवन का उपसंहार है
लंका हो या अवध
उसके लिए एक-सा कारागार है।
वर्ष-दर-वर्ष, अपने प्रतिशोध की तृप्ति के लिए
वह टालता आया है हर्ष
वह जो बनना चाहता है युग का आदर्श :
अंदर से एक साधारण आदमी निकल आया है
उसे महसूस होता है,
इतनी क़ीमत चुका कर
उसने जिस सत्य को पाया है,
वह सत्य नहीं, महज़ उसकी छाया है।
लेकिन अब उसे मालूम है,
यह यात्रा के अंत की शुरुआत है
(भले ही यह उसकी प्रियतमा पर
उसी दुर्दम दैत्य—अपवाद—का आघात है)
तीन
कौन था वह जिसकी जय-यात्रा हम
इतने उत्साह, इतने जोश से मनाते हैं?
उसकी विजय, विजय नहीं, एक झुका हुआ माथ है
जिसकी सबसे बड़ी पराजय एक परित्यक्त हाथ है
वह जो अपनी शंका के आगे,
प्रवाद के सम्मुख
ख़ामोश हो गया
वह जो सत्ता का निर्विकार मुखोश हो गया
कौन था वह जिसकी जय-यात्रा हम
वर्ष दर वर्ष मनाते हैं।
चार
हर साल। साल-दर-साल। हम एक आकृति
घृणा से रच कर अपने अंदर-ही-अंदर बनाते हैं
फिर जा कर उसे हम जला आते हैं
कौन था वह जिसकी सूरत
हम आज भी अपने अंदर पाते हैं?
स्रोत :
पुस्तक : कुल जमा-1 (पृष्ठ 146) रचनाकार : नीलाभ प्रकाशन : शब्द प्रकाशन संस्करण : 2012
9. मंदोदरी — डॉ. पंकज
रावण के महल की नीरव दीवारों में,
आज भी गूँजती है मेरी सिसकियाँ।
शक्ति का मद, अहंकार का ज्वार,
जिसने परिवार और साम्राज्य डुबो डाला।
मैंने कितनी बार कहा था—
“स्वामी! यह नीति नहीं, अनैतिकता है,
सीता अपहरण से विजय नहीं,
सिर्फ विनाश उपजता है।”
पर मेरी वाणी,
उसके शौर्य के शोर में दब गई।
विजय की जगह आज
हवन-कुंड में धधकते पुतलों में जलती है
रावण की छवि।
दशहरे की भीड़ में
जब लोग हँसते हैं, आतिशबाज़ियाँ छोड़ते हैं,
तब मैं सोचती हूँ—
क्यों नहीं कोई जलाता
उस अहंकार को,
जो रावण के भीतर था?
क्या हर युग में
सीता का अपमान ही होगा
और मंदोदरी की चेतावनी
अनसुनी रह जाएगी?
मैं आज भी खड़ी हूँ,
विधवा होकर, इतिहास की परछाइयों में—
लोग पुतले जलाते हैं,
पर सबक नहीं सीखते।
10. उर्मिला वियोग
चुप रह गई हूँ मैं, ये सफ़र कैसा हुआ,
वह चला राम संग, और घर कैसा हुआ।
रातें तो गुज़रीं बस उसके नाम पर,
नींद का भी मुझसे ख़ुदा कैसा हुआ।
सुनती रही मैं वन की कथाएँ हर घड़ी,
पर संगिनियों का भी सहारा कैसा हुआ।
पलकें थकीं तो आँसुओं से भीग गईं,
सपनों का ताबीर में धुँधलका सा हुआ।
उर्मिला कहे, विरह में हूँ पर स्थिर भी,
पति का धर्म निभा, मेरा तप कैसा हुआ।
— डॉ. अविनीश प्रकाश सिंह