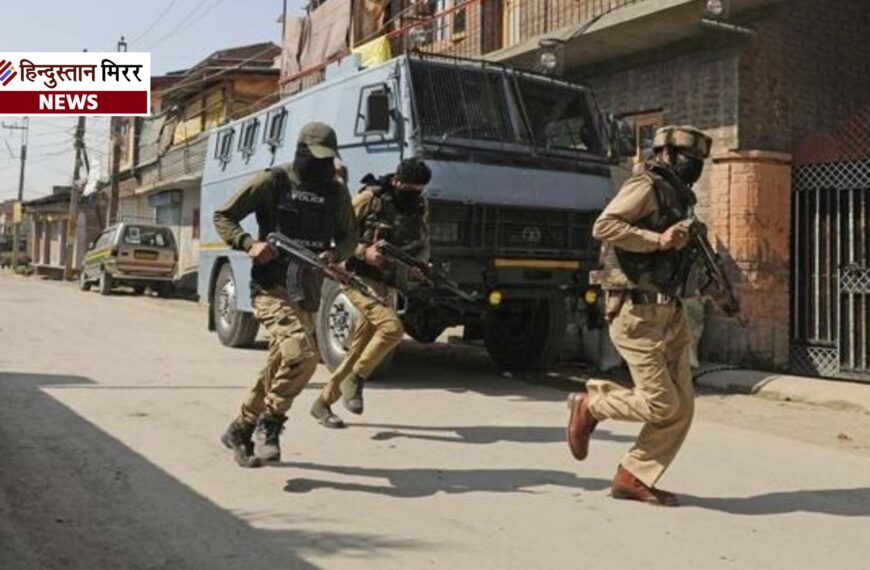बुटा सिंह
सहायक आचार्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
1. प्रस्तावना: भारत के हृदय में बसे गाँव और खेती
भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक संरचना की जड़ें उसके ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था में निहित हैं। कृषि केवल उत्पादन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, जीवनमूल्यों, आचार-विचारों और सामुदायिक लोकाचार का मूल आधार है। गांधीजी ने इसीलिए कहा कि “भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है।”
वर्तमान में भी लगभग 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और 50% से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि व कृषि-आधारित गतिविधियों पर निर्भर हैं। हालांकि GDP में कृषि का योगदान लगभग 16–18% ही है, पर ग्रामीण भारत का महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है—यह देश के खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, पशुधन, वन, जल संसाधन और जैव विविधता को समेटे हुए है।
इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के बाद भारतीय कृषि और ग्रामीण संरचना लगातार संक्रमण, पुनर्गठन और रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही है जिसमें तकनीक, बाजार, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव, पलायन, और सरकारी नीतियाँ महत्वपूर्ण कारक बनकर उभर रहे हैं। यह आलेख इन्हीं बहुआयामी परिवर्तनों और चुनौतियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: हरित क्रांति से लेकर वर्तमान कृषि सुधार तक
2.1 हरित क्रांति का उद्भव और प्रभाव
हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को पारंपरिक आत्मनिर्भरता के संकट से निकालकर आधुनिक उत्पादन प्रणाली की ओर मोड़ा। HYV बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई विस्तार और मशीनरी के सम्मिलित उपयोग ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया।
इसके सकारात्मक प्रभाव—
- उत्पादन में 3–4 गुना वृद्धि
- खाद्य आयात से मुक्ति
- पश्चिमोत्तर भारत में कृषि-समृद्धि का उभार
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विस्तार
इसके दुष्परिणाम—
- मिट्टी की उर्वरता में गिरावट
- भूजल दोहन में वृद्धि
- क्षेत्रीय असमान आर्थिक विकास
- रसायनों के कारण स्वास्थ्य व पर्यावरणीय संकट
हरित क्रांति ने कृषि का ध्यान ‘अधिक उत्पादन’ पर केंद्रित किया, लेकिन ‘आय’, ‘स्थिरता’ और ‘समानता’ के मुद्दे उपेक्षित रह गए।
2.2 भूमि का विखंडन और उसका प्रभाव
भारतीय समाज मुख्यतः पारिवारिक कृषि पर आधारित रहा है। विरासत कानूनों के कारण भूमि पीढ़ी-दर-पीढ़ी विभाजित होती गई—
- 86% किसान छोटे और सीमांत
- औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर
- मशीनीकरण महँगा
- उत्पादन लागत अधिक
छोटी जोतें भारतीय कृषि की प्रमुख संरचनात्मक चुनौती हैं, जिसके कारण ‘आर्थिक पैमाने’ (economies of scale) का लाभ नहीं मिल पाता।
3. ग्रामीण समाज की संरचना और अंतर्निहित चुनौतियाँ
3.1 कर्ज, जोखिम और कृषि संकट
भारतीय कृषि जोखिमों से भरा क्षेत्र है—मौसम, कीट, बाजार भाव, भंडारण की कमी, ऊँची लागत और कम लाभ। इसके कारण—
- किसानों का औसत ऋण बढ़ता जा रहा है
- सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण कम मिलता है
- साहूकारों पर निर्भरता बढ़ती है
कर्ज संकट केवल आर्थिक समस्या नहीं; यह सामाजिक-मानसिक संकट भी है। कई राज्यों में किसान आत्महत्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो कृषि व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों की ओर संकेत करती है।
3.2 कृषि का नारीकरण: महिलाओं की उभरती भूमिका
पुरुषों के शहरी पलायन और कृषि मजदूरी के बदलते स्वरूप के कारण महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।
महिलाएँ—
- 70% से अधिक खेत मजदूरी करती हैं
- 50% से अधिक पशुपालन कार्य करती हैं
- बीज चयन, निराई, कटाई का बड़ा हिस्सा करती हैं
परंतु अब भी:
- जमीन पर उनका स्वामित्व केवल 13% के आसपास
- निर्णय प्रक्रिया में सीमित भूमिका
- संस्थागत कर्ज तक कम पहुँच
यह स्थिति कृषि को लैंगिक न्याय के दृष्टिकोण से कमजोर बनाती है।
3.3 पलायन: ग्रामीण-शहरी संबंधों का नया गतिशास्त्र
पलायन के पीछे प्रमुख कारण—
- गाँव में रोजगार की कमी
- स्वास्थ्य व शिक्षा की अपर्याप्तता
- कृषि में अनिश्चितता
परिणाम—
- गाँव में श्रम की कमी
- बुजुर्ग किसान ही कृषि में रह जाते हैं
- शहरों में अनौपचारिक बस्तियों का विस्तार
- सामाजिक संरचना में बदलाव
ग्रामीण विकास की नीतियों को पलायन को ‘कम करने’ और गाँव में ‘स्थानीय रोजगार सृजन’ पर केंद्रित होना आवश्यक है।
4. पर्यावरणीय परिवर्तन और कृषि: एक बढ़ता संकट
4.1 जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ
भारतीय कृषि 60% तक वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन ने—
- बाढ़
- सूखा
- ओलावृष्टि
- तापमान वृद्धि
- बेमौसम वर्षा
जैसे संकट बढ़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दशकों में गेहूँ-धान की उपज 10–20% तक घट सकती है।
4.2 जल संकट और संसाधन प्रबंधन
भारत विश्व के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त देशों में से एक है।
आवश्यक है—
- माइक्रो इरिगेशन का विस्तार
- तालाब, जोहड़, नाड़ियाँ, बावड़ियों का पुनर्जीवन
- भूजल पुनर्भरण
- फसल विविधीकरण (चावल की जगह मोटा अनाज)
इन प्रयासों के बिना कृषि दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं बन सकती।
4.3 स्थायी कृषि: जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बदलाव
रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के कारण जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
इसके फायदे—
- उत्पादन लागत कम
- मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर
- बाजार में उच्च मूल्य
- स्वास्थ्य लाभ
आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक कृषि (APCNF) और सिक्किम की ऑर्गेनिक नीति इसके बड़े उदाहरण हैं।
5. आर्थिक सुधार, तकनीकी नवाचार और कृषि का आधुनिकीकरण
5.1 कृषि का बाजार से समन्वय
किसानों की आय वृद्धि के लिए उन्हें बाजार से सीधे जोड़ना आवश्यक है।
- e-NAM: एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
- फसल बीमा
- गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण
इन साधनों से किसानों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ती है।
5.2 स्मार्ट और डिजिटल कृषि
भारत में डिजिटल खेती तेजी से बढ़ रही है—
- ड्रोन द्वारा छिड़काव
- मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड
- सैटेलाइट आधारित सलाह
- एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान
- कृषि ऐप्स
ये नवाचार लागत घटाते हैं और दक्षता बढ़ाते हैं।
5.3 मूल्य संवर्धन और एग्रो-उद्योग
कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर है—
- आटा मिल, मसाला प्रोसेसिंग
- डेयरी, कोल्ड चेन
- फल-सब्ज़ी आधारित उत्पाद
- ग्रामीण उद्यमिता
इससे रोजगार, स्थानीय उद्योग और किसानों की आय तीनों बढ़ते हैं।
6. नीतिगत हस्तक्षेप और ग्रामीण विकास मॉडल
6.1 FPOs: सामूहिक शक्ति का निर्माण
FPOs छोटे किसानों को—
- सस्ती खरीद
- समूह बिक्री
- तकनीकी प्रशिक्षण
- बाजार तक सीधी पहुँच
प्रदान करते हैं।
यह कृषि में ‘कलेक्टिव कैपिटल’ का उदय है।
6.2 ग्रामीण आजीविका विविधीकरण
NRLM, SHGs और कौशल विकास मिशनों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ‘बहुआयामी’ बनाया है।
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- बागवानी
- कुटीर उद्योग
- हस्तशिल्प
इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है।
6.3 मानव पूंजी का सुदृढ़ीकरण
ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल प्रशिक्षण का सुदृढ़ होना अनिवार्य है।
- बेहतर विद्यालय
- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- डिजिटल साक्षरता
- कृषि आधारित प्रशिक्षण
मानव पूंजी कृषि और ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ है।
7. निष्कर्ष: एक स्थायी, समावेशी और समृद्ध ग्रामीण भारत की ओर
भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन आज रूपांतरण के निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
भविष्य के लिए आवश्यक है—
- टिकाऊ कृषि पद्धति
- जल संरक्षण आधारित खेती
- महिला किसानों को अधिकार
- तकनीक आधारित उत्पादन
- बाजार से बेहतर जुड़ाव
- ग्रामीण उद्योग और रोजगार
- मानव पूंजी में निवेश
जब तक गाँव मजबूत नहीं होंगे, भारत आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्थायी नहीं बन सकता। अतः कृषि और ग्रामीण जीवन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और भविष्य की आधारशिला हैं।