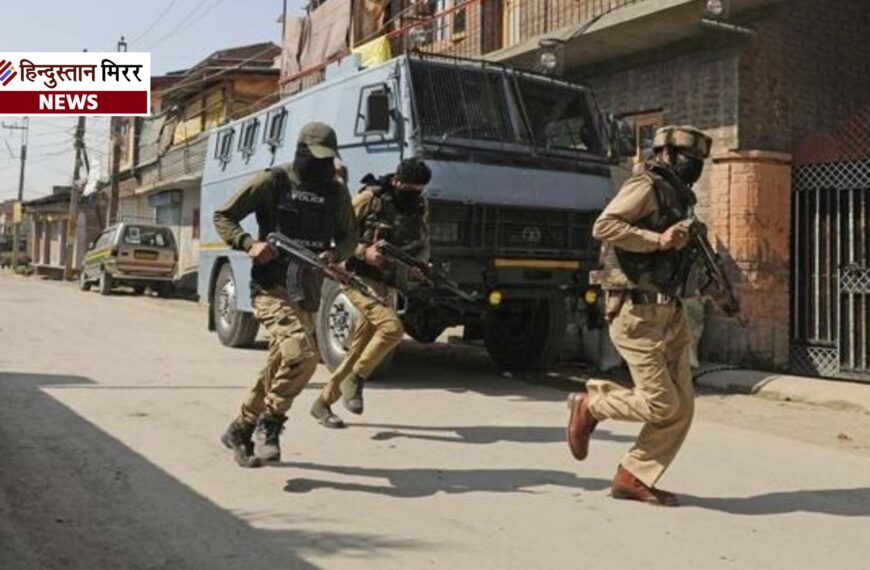बुटा सिंह
सहायक आचार्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
सदियों से, गाँवों की चौपाल (सामुदायिक केंद्र) ग्रामीण संवाद, निर्णय लेने और अनौपचारिक शासन का केंद्र रही है। आज, भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ डिजिटल क्रांति इस पारंपरिक चौपाल की शक्ति को हर ग्रामीण नागरिक की चौखट (देहली, घर) तक पहुँचा रही है। यह आलेख ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण, शासन और डिजिटल क्रांति के इस जटिल और परिवर्तनकारी अंतर्संबंध का विस्तार से विश्लेषण करता है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि डिजिटल तकनीकें न केवल सरकारी सेवाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचा रही हैं, बल्कि कैसे यह ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं और हाशिये पर पड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय शासन की पारदर्शिता को बढ़ावा दे रही हैं।
I. प्रस्तावना: परिवर्तन की आवश्यकता और पृष्ठभूमि
भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, जिसकी लगभग 65% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। स्वतंत्रता के बाद से, ग्रामीण विकास हमेशा एक चुनौती रहा है, जहाँ गरीबी, सीमित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच, और खराब बुनियादी ढाँचा प्रमुख बाधाएँ रही हैं। पारंपरिक शासन व्यवस्था अक्सर धीमी, नौकरशाही वाली और अपारदर्शी रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम नागरिक तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाता था।
ऐतिहासिक रूप से, पंचायती राज व्यवस्था (73वाँ संवैधानिक संशोधन) ने विकेंद्रीकृत शासन की नींव रखी, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति ग्राम पंचायतों को मिली। हालांकि, प्रभावी परिणामों के लिए एक मजबूत पारदर्शिता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता थी।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015 में शुरू) ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। यह कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक मुख्य उपयोगिता के रूप में प्रदान करना।
- मांग पर शासन और सेवाएँ प्रदान करना।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना।
‘चौपाल से चौखट तक’ की यात्रा इसी परिवर्तन को दर्शाती है – सामूहिक चर्चा से लेकर व्यक्तिगत पहुँच और भागीदारी तक, जहाँ सूचना और सेवाएँ अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध हैं।
II. डिजिटल क्रांति और ग्रामीण सशक्तिकरण
डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ ग्रामीण भारत में सशक्तिकरण की एक नई लहर ला रही हैं, जो न केवल आर्थिक स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा दे रही हैं।
A. वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण
जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति: यह भारत की डिजिटल क्रांति का मूल स्तंभ है।
- जन धन: प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता।
- आधार: प्रत्येक नागरिक की अद्वितीय डिजिटल पहचान।
- मोबाइल: कनेक्टिविटी और सेवाओं तक पहुँच।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): सरकारी सब्सिडी और लाभ अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं, जिससे रिसाव (leakage) और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। मनरेगा मजदूरी, गैस सब्सिडी, और विभिन्न पेंशन योजनाएँ अब DBT के माध्यम से वितरित होती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई है और जरूरतमंदों तक उनका पूरा हक़ पहुँच रहा है।
UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) क्रांति: ग्रामीण बाजारों और छोटे व्यवसायों ने UPI को तेजी से अपनाया है। किसान, छोटे दुकानदार और कारीगर अब कैशलेस लेनदेन कर रहे हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ सुगम हुई हैं और वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ गए हैं।
B. ज्ञान और सूचना का लोकतंत्रीकरण
डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से, ग्रामीण समुदायों को वह जानकारी मिल रही है, जो पहले केवल शहरों तक सीमित थी।
- शिक्षा: स्वयं (SWAYAM) और दीक्षा (DIKSHA) जैसे प्लेटफॉर्म ग्रामीण छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री प्रदान कर रहे हैं, जिससे शहरी-ग्रामीण शिक्षा अंतराल को कम करने में मदद मिल रही है।
- कृषि: ई-नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। किसान अब मौसम की भविष्यवाणी, मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी और नवीनतम कृषि तकनीकों को सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य सेवा: टेलीमेडिसिन पहल ने दूर-दराज के गाँवों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुँच सुनिश्चित की है, जिससे ग्रामीणों को लंबी दूरी की यात्रा से मुक्ति मिली है और तत्काल चिकित्सा सहायता संभव हुई है।
C. महिला सशक्तिकरण में डिजिटल भूमिका
शोध बताते हैं कि डिजिटल तकनीकों को अपनाने में ग्रामीण महिलाएं पुरुषों की तुलना में आगे निकल रही हैं।
- डिजिटल साक्षरता: सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं को स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया है।
- आजीविका के अवसर: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। महिलाएँ अब अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे जीईएम – GeM पोर्टल) पर बेचकर एक बड़ा बाज़ार प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे उद्यमी बन रही हैं (लखपति दीदी पहल)।
- राजनीतिक भागीदारी: डिजिटल उपकरणों से महिलाएं पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकती हैं और सार्वजनिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं, जिससे उनका राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है।
III. शासन में सुधार: ई-गवर्नेंस की भूमिका
डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण शासन के चेहरे को बदल दिया है, जिससे यह अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बन गया है।
A. ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण
ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP): यह परियोजना ग्रामीण प्रशासन को कंप्यूटरीकृत करके ग्राम पंचायतों को सशक्त बना रही है।
- ग्राम स्वराज पोर्टल: यह योजना और बजट बनाने, कार्यों के रिकॉर्ड रखने, और वित्तीय प्रबंधन में पंचायतों की मदद करता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है।
- सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज़ अब कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से गाँवों में उपलब्ध हैं। CSCs ग्रामीण उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं और ‘चौखट’ तक सरकारी सेवाओं की एकल-खिड़की पहुँच प्रदान करते हैं।
B. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP): इस कार्यक्रम के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मदद मिली है। भू-नक्शों का कंप्यूटरीकरण और अभिलेखों का ऑनलाइन प्रकाशन भ्रष्टाचार को कम करता है और किसानों को अपनी संपत्ति को ऋण के लिए संपार्श्विक (Collateral) के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
C. जवाबदेही और सहभागी शासन
- सरकारी डैशबोर्ड और निगरानी: विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को सार्वजनिक डैशबोर्ड (जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण या मनरेगा) पर वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है। यह पारदर्शिता अधिकारियों को जवाबदेह बनाती है।
- सहयोगी मंच: डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीणों को सरकार को सीधे प्रतिक्रिया देने, शिकायतें दर्ज करने और नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देते हैं, जिससे सहभागी लोकतंत्र मजबूत होता है।
IV. चुनौतियाँ और आगे की राह
डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण भारत में ‘चौपाल से चौखट तक’ की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है।
A. डिजिटल डिवाइड (अंतराल)
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच का एक बड़ा अंतराल मौजूद है।
- बुनियादी ढाँचा: यद्यपि भारतनेट परियोजना हर ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन अंतिम-मील कनेक्टिविटी, बिजली की अस्थिरता और स्मार्टफोन की सामर्थ्य अभी भी बाधाएँ हैं।
- डिजिटल कौशल: कई ग्रामीण नागरिकों में, विशेषकर वृद्धों और हाशिये के समुदायों में, डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है।
B. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
डिजिटल लेनदेन और व्यक्तिगत डेटा के बढ़ते उपयोग के साथ, ग्रामीण नागरिकों के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्हें फिशिंग और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए निरंतर जागरूकता और प्रशिक्षण आवश्यक है।
C. भाषा बाधा
अधिकांश डिजिटल सेवाएँ और सामग्री अभी भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में या कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। बहुभाषी और स्थानीय भाषा सामग्री की कमी डिजिटल सेवाओं को अपनाने में बाधा डालती है।
V. निष्कर्ष: एक समावेशी भविष्य की ओर
‘चौपाल से चौखट तक’ का सफर ग्रामीण भारत के लिए सिर्फ तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की गाथा है। डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण शासन को विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और कुशल बनाया है। इसने नागरिकों को जानकारी और सेवाओं तक सीधी पहुँच देकर एक ‘सेवा प्रदाता’ से ‘शक्तिशाली भागीदार’ में बदल दिया है।
भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वाकांक्षा को तभी साकार किया जा सकता है, जब देश का ग्रामीण हृदय पूरी तरह से डिजिटल रूप से सशक्त हो। चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बुनियादी ढाँचे के निवेश (जैसे 5G और BharatNet) को बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में व्यापक बनाना, और डिजिटल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
डिजिटल चौपाल वह नया सार्वजनिक मंच है, जहाँ ग्रामीण भारत का भविष्य रचा जा रहा है—एक ऐसा भविष्य जो समावेशी, समान और स्व-निर्भर है। यह क्रांति भारत के लोकतंत्र को उसकी सबसे गहरी जड़ों तक मजबूत कर रही है, यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और समृद्धि के अवसर हर चौखट पर दस्तक दें। यह परिवर्तन सिर्फ शुरुआत है; आने वाले दशक में, डिजिटल तकनीकें ग्रामीण भारत के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देंगी, जिससे एक सच्चे ‘अमृत काल’ की नींव रखी जाएगी।