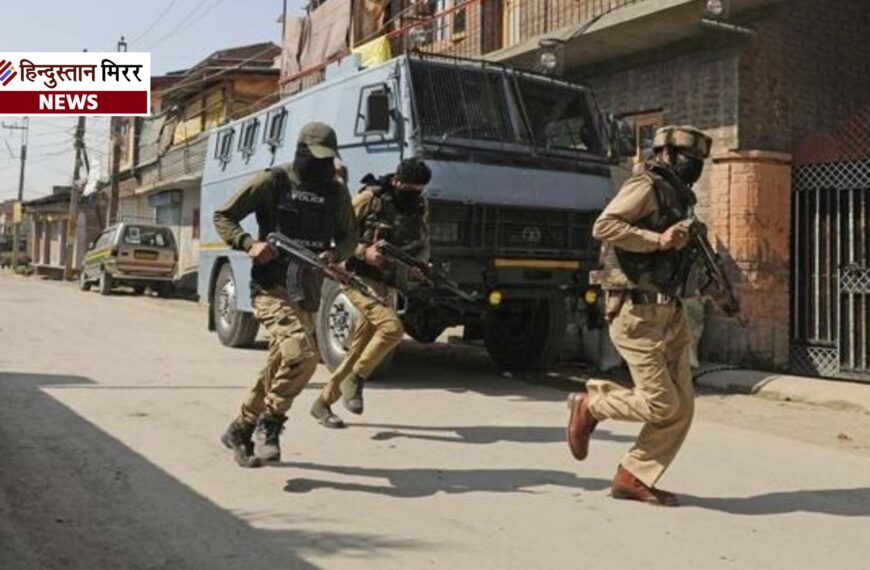बुटा सिंह
सहायक आचार्य,
ग्रामीण विकास विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
“भारत का भविष्य उसके गाँवों में बसता है।” — महात्मा गांधी
भारतीय लोकतंत्र का वास्तविक चेहरा उसके गाँवों में दिखाई देता है, और इन गाँवों की धड़कन पंचायती राज संस्थाओं में सुनाई देती है। इन संस्थाओं के केंद्र में ग्राम प्रधान (सरपंच) का पद है, जो केवल प्रशासनिक इकाई का मुखिया नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं, अधिकारों और स्वप्नों का संवाहक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने ग्राम प्रधान को संवैधानिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र की जड़ों को गाँव की मिट्टी में और गहराई तक रोपा। यह बदलाव केवल संरचनात्मक न होकर सामाजिक-राजनीतिक भी था, जिसने स्वशासन और सहभागिता की अवधारणा को साकार किया।

जैसा कि ग्राम स्वराज के पक्षधर गांधीजी का मानना था — “स्वराज्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठकर अपनी आत्मा को पहचान सके और गाँव स्वयं अपना शासन कर सके।” इस दृष्टिकोण से ग्राम प्रधान की भूमिका आज के भारत में और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
1. विकास योजनाओं का शिल्पकार: प्रशासन से परे एक नेतृत्व
ग्राम प्रधान की भूमिका केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का वास्तु तैयार करना है। वे उस नेतृत्वकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं, जो गाँव की बुनियादी ज़रूरतों को पहचानकर उन्हें वास्तविकता में बदलते हैं।
- आर्थिक सशक्तिकरण: मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत ग्राम प्रधान स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करते हैं। यह केवल कार्य का वितरण नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका का संरक्षण है। सामुदायिक संपत्तियों—तालाब, नहर, सड़क—का निर्माण गाँव की आत्मनिर्भरता की नींव रखता है।
- आवास और स्वच्छता: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान न केवल लाभार्थियों की पहचान करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाते हैं। खुले में शौच मुक्त गाँव केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से भी जुड़ा है।
- आधारभूत संरचना: पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइटें और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ग्राम प्रधान की सक्रियता से ही संभव होती है। यह बुनियादी ढाँचा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है।
2. वित्तीय पारदर्शिता और सुशासन का प्रहरी
सुशासन का आधार पारदर्शिता है, और ग्राम प्रधान इस व्यवस्था के वित्तीय प्रहरी होते हैं।
- कोष प्रबंधन: 14वें और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान का सही आवंटन ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। स्थानीय राजस्व और सामुदायिक संपत्तियों से प्राप्त आय का सदुपयोग ग्राम पंचायत की आत्मनिर्भरता को पुष्ट करता है।
- सामाजिक लेखा-परीक्षा: ग्राम सभा की बैठकों में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीणों को सीधी भागीदारी का अवसर भी देता है। यह लोकतंत्र की जड़ में निहित “जन द्वारा, जन के लिए” की भावना को मूर्त करता है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): ग्राम प्रधान इस योजना का नेतृत्व करते हैं, जो गाँव की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होती है। यहाँ विकास किसी बाहरी आदेश का परिणाम नहीं, बल्कि सामुदायिक सहमति का प्रतिफल होता है।
3. सामाजिक न्याय और सद्भाव का संवाहक
ग्राम प्रधान केवल योजनाओं का प्रशासक नहीं, बल्कि गाँव के सामाजिक ताने-बाने का संरक्षक भी है।
- विवाद निपटारा: स्थानीय विवादों—जमीन, परिवार, सीमाओं—में ग्राम प्रधान एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह कार्य करते हैं। उनके निर्णय औपचारिक न्यायालयों की तुलना में सरल, त्वरित और सामाजिक स्वीकृति से युक्त होते हैं।
- हाशिये पर खड़े वर्गों का उत्थान: अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान तभी सार्थक बनते हैं जब उनका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचे।
- सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ संघर्ष: बाल विवाह, दहेज और जातिगत भेदभाव जैसी प्रथाओं के विरुद्ध ग्राम प्रधान की जागरूकता और प्रयास उन्हें एक समाज सुधारक का दर्जा देते हैं।
4. संवैधानिक ढाँचे और स्थानीय यथार्थ का सेतु
73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो दिया, किंतु उनकी वास्तविक शक्ति राज्यों की इच्छाशक्ति और संसाधनों पर निर्भर है। इस स्थिति में ग्राम प्रधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद सेतु की भूमिका निभाते हैं।
- शासन से संपर्क: ग्राम प्रधान गाँव की समस्याओं को ब्लॉक और जिला स्तर पर पहुँचाते हैं, और सरकारी विभागों के साथ तालमेल स्थापित करते हैं।
- जन प्रतिनिधित्व: वे ग्रामीणों के विचारों और समस्याओं को उच्च स्तर तक ले जाकर लोकतंत्र को bottom-up ढाँचा प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष: लोकतंत्र की रीढ़ और भविष्य का पथप्रदर्शक
ग्राम प्रधान का पद केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा है। वे योजनाओं के शिल्पकार, वित्तीय पारदर्शिता के प्रहरी, सामाजिक न्याय के संवाहक और संवैधानिक ढाँचे के सेतु हैं। चुनौतियाँ अवश्य हैं—सीमित संसाधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा का अभाव—लेकिन इन सबके बावजूद, एक जागरूक और सशक्त ग्राम प्रधान “सुशासन” की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकता है।
जैसा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था— “लोकतंत्र केवल सरकार की संरचना नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का तरीका है।” ग्राम प्रधान इसी लोकतांत्रिक जीवन-शैली को गाँव के स्तर पर साकार करते हैं।
इस प्रकार, पंचायती राज से सुशासन तक की यात्रा में ग्राम प्रधान की भूमिका आधारभूत और निर्णायक है। गाँवों का विकास केवल स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है, और यही नेतृत्व भारत के आत्मनिर्भर और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।